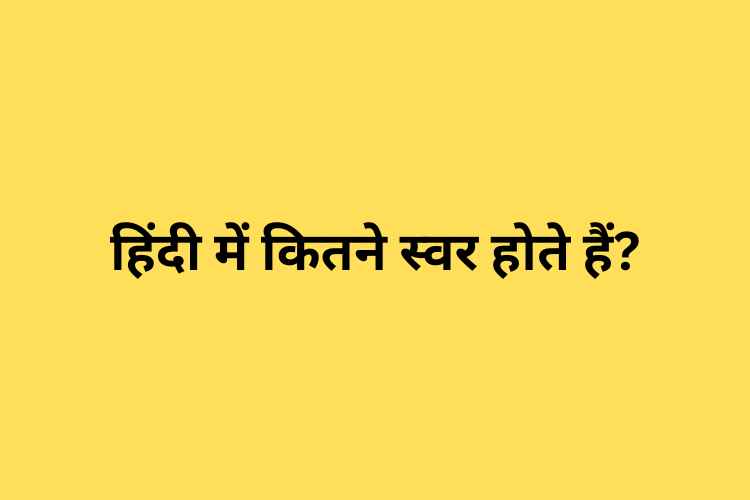ऐसे वर्ण जिन का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहा जाता है, किसी भी Swar की ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि आवरण की सहायता नहीं होती है, वायु मुख विवर में बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है. हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं, जैसे अ , आ , इ , ई , उ , ऊ , ऋ , ए , ऐ , ओ , औ आदि.
स्वर के कितने प्रकार होते हैं?
स्वर्ग के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं-
(1) मूल स्वर:– अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ
(2) संयुक्त स्वर:- ऐ (अ +ए) और औ (अ +ओ)
मूल स्वर के प्रकार
मूल स्वर के तीन प्रकार होते है –
- ह्स्व स्वर
- दीर्घ स्वर
- प्लुत स्वर
(i) ह्स्व स्वर –
हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें ह्स्व स्वर कहते हैं, हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से चार प्रकार के ह्स्व स्वर होते है – अ आ उ ऋ.
(ii) दीर्घ स्वर –
हिंदी व्याकरण के वे वर्ण या स्वर जिन का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं.
दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
दीर्घ स्वर मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं – आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ.
दीर्घ स्वर दो शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे-
आ = (अ +अ )
ई = (इ +इ )
ऊ = (उ +उ )
ए = (अ +इ )
ऐ = (अ +ए )
ओ = (अ +उ )
औ = (अ +ओ )
(iii) प्लुत स्वर –
वह स्वर या वर्ण जिन का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है. उसे लुप्त स्वर्ग कहते हैं. प्लुत स्वरों में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है. जिसके कारण इनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है.
संयुक्त स्वर :-
वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं. इनकी संख्या 5 होती है जो इस प्रकार है- ए, ऐ, ओ, औ, ऋ
उदाहरण :– अ + आ = ए , अ + ए = ऐ , अ + उ = ओ , अ + ओ = औ इत्यादि.
स्वरों का वर्गीकरण
स्वरों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है कुछ इस प्रकार से:–
मात्रा के आधार पर –
ह्रस्व स्वर – अ, इ, उ, ऋ
दीर्घ स्वर – आ, ई, ऊ, ए,ऐ,ओ,औ
मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर-
विवृत – आ
अर्द्ध विवृत – ऐ, औ
अर्द्ध संवृत – ए, ओ
संवृत – इ, ई, उ,ऊ
जीभ के प्रयोग के आधार पर –
अग्र स्वर- इ, ई, ए, ऐ
मध्य स्वर – अ
पश्च स्वर – आ, उ, ऊ, ओ, औ
ओठों की स्थिति के आधार पर –
अवर्तुल या सहज – इ, ई, ए, ऐ
वर्तुल – उ,ऊ, ओ, औ
अर्द्धवर्तुल – आ
जीह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर –
शिथिल – अ, इ, उ
कठोर – आ, इ, उ
स्थान के आधार पर-
कंठ्य – अ, अः
तालव्य – इ
मूर्धन्य – ऋ
ओष्ठ्य – उ, ऊ
अनुनासिक – अं